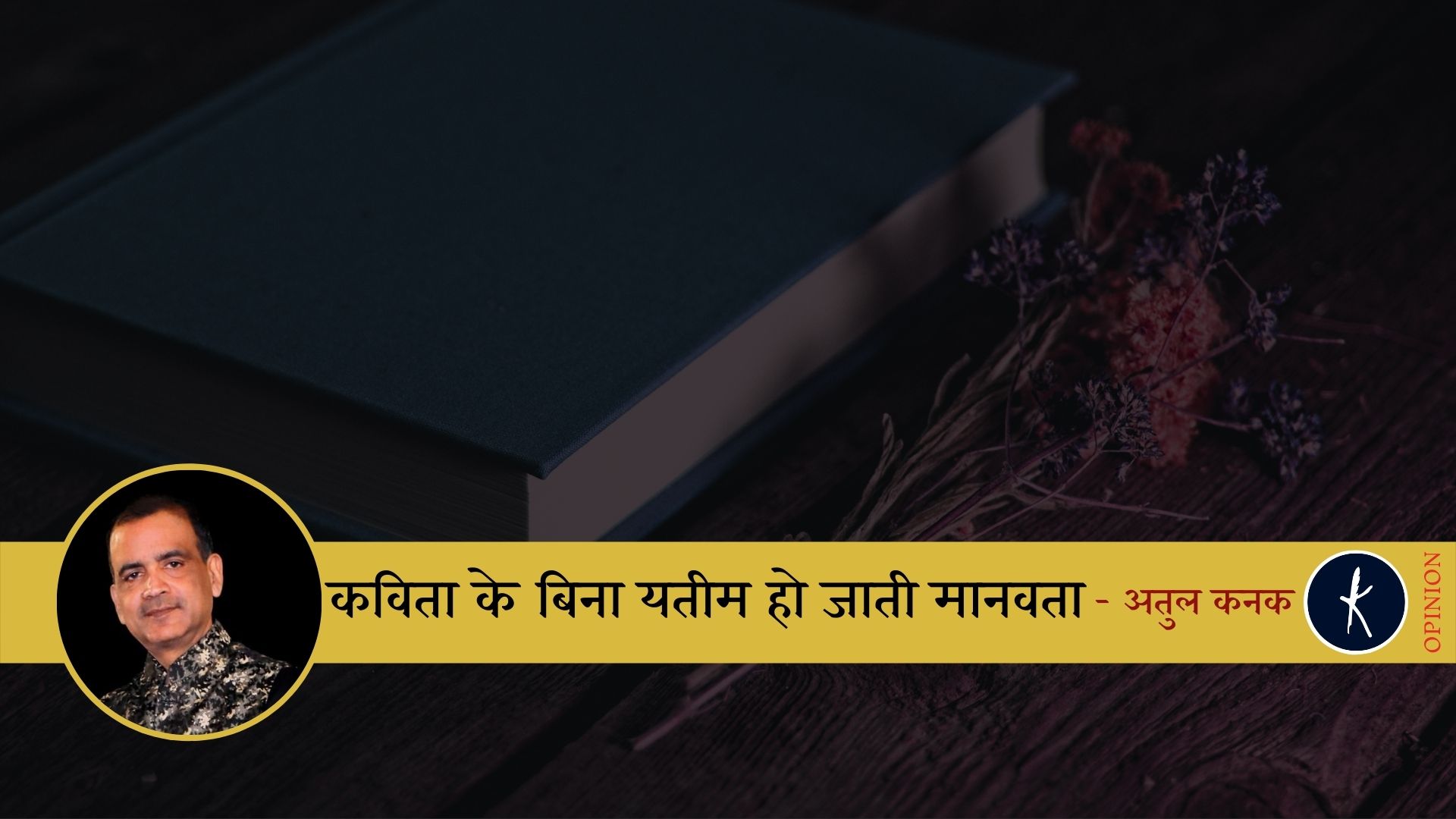
कविता ने हर युग में मनुष्य को जीने की शक्ति दी है और जीवन की सकारात्मकता के प्रति आस्थावान बनाया है। यह अलग बात है कि हर दौर में नकारात्मक प्रवृत्तियों को कविता का मुखर होना अप्रिय प्रतीत हुआ है। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब किसी कवि को कुछ कविताओं के लिये या किसी कविता को उसके विद्रोही स्वर के लिये प्रतिबंधित किया गया या रचनाकार को प्रताड़ित किया गयां। लेकिन कविता में मुखर होता विरोध भी जीवन की सर्जनात्मक प्रवृत्तियों का समर्थन ही होता है। याद करिये कि जब बीकानेर के राणा फतेहसिंह ब्रिटिश दरबार में हाजिरी लगाने के लिये जाने लगे तो किस तरह केसरीसिंह बारहठ ने उन्हें अपना कुल गौरव स्मरण कराते हुए चेतावनी रा चूंगट्या नाम से दोहों की एक श्रृंखला लिखी थी और वो दोहे राणा को प्रेषित कर दिये थे। उन दोहों को पढ़ने के बाद राणा ने ब्रिटिश दरबार में जाने का अपना ही निर्णय रद्द कर दिया था। भारत में तो कवियों को उनकी सर्जनात्मक चेतना के कारण ही ऋषि तुल्य माना गया है। हमारे प्राचीन वांग्मय में कवि का एक पर्यायवाचख्ी ऋषि भी बताया गया है। ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जब स्वयं शासकों ने अपने दरबारी कवियों के सम्मान में उनकी पालकियों को कंधे पर ढोया है।
लेकिन बाजारवाद ने हर प्रवृत्ति को इस हर तक जकड़ लिया है कि हम अपना स्वार्थ साबित करने के लिये सूरज के उजाले में भी अधेरों के बिम्ब खोजने के आदी हो गये हैं। चूँकि कविता अपने कथ्य और अपने शिल्प में लोगों के मन को सहज ही आकर्षित करती है, इसलिये हर कोई कविता को अपनी अभिव्यक्ति के हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। एक कविता जब किसी एक पक्ष की ताकत बनती प्रतीत होती है, तो उस पक्ष के विरोध कविता का भी विरोध करने पर आमादा हो जाते हैं। यह कविता की ताक़त है कि इसे बेबस बनाने की कोशिशें भी होती रही हैं। लेकिन कविता हर युग में कमजोरों के साहस की मशाल प्रज्वलित करती रही है। भले ही कविता के ‘होई सोई जो राम रचि राखा- स्वर को प्रसाारित कर मनुष्य को यथास्थितिवादी बनाने का प्रयास भी किया लेकिन यह कविता ही थी जिसने कठिन पलों में भी मनुष्य को कर्म की चेतना देते हुए समझाया -‘‘कर्म प्रधान विश्व करि राखा/ जो जस करिहे सो तस फल चाखा।’’
कविता कतिपय नकारात्मक प्रवृत्तियों को हर युग में चुनोती देती सी प्रतीत होती है। चूँकि कविता का भावबोध और उसके शिल्प का सौंदर्य सीधे मनुष्य की आत्मा के द्वार पर दस्तक देता है, इसलिये कविता के दम पके प्रयास भी विश्व इतिहास में कम नहीं हुए। याद करिये कि कैसे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की मूल पंक्ति -‘‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’’ आपातकाल के बाद जन आंदोलनों की प्रणेता बन गई थी। यह वह दौर था, जब अनेक ताकतवर कलमकार सत्ता की कार्यवाहियों की आशंका से डरकर कथित तौर पर निष्पेक्ष हो गये थे और मुक्तिबोध की एक पंक्ति ‘पार्टनर तुम्हारी पॉलीटिक्स क्या है’’ ऐसे लोगों पर तीखा प्रहार करने लगी थी। एक चिंतक ने सही कहा है कि कविता किसी क्रांति का नेतृत्व भले ही नहीं करे, लेकिन क्रांति की चेतना ज़रूर जगा सकती है। आजादी की लड़ाई के दिनों में बांकीदास ने ‘आया इंगरेज मुलक रे ऊपर’ और सूर्यमल्ल मिश्रण ने ‘इला न देणी आपणी’ जैसी कविताऐं लिखकर राजस्थान में ऐसी ही चेतना को तो जागृत किया था। किसी कलमकार की सर्जना से नकारात्मक व्यवस्था किस हद तक भयभीत हो सकती है, इसे राजस्थान के सागरमल गोपा के उदाहरण से जाना जा सकता है। सागरमल गोपा को आजादी के पूर्व ‘जैसलमेर में गुण्डा राज’ नामक पुस्तक लिखने के कारण पहले कारावास में डाला गया और फिर कारावास में ही जिन्दा जला दिया गया। लेकिन ऐसे जुल्मों से कविता के स्वर कहाँ मौन होते हैं? रामप्रसाद बिस्मिल को भले ही फाँसी पर चढ़ा दिया गया लेकिन उनकी पंक्तियाँ ‘सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है/ देखना है ज़ोर कितना बाजू-ए- कातिल में है’ आजादी के दीवानों के लिये प्रेरणा का स्रोत बन गईं। कविता की ताकत ही ऐसी है कि वो जब उमंग जगाती है तो हर बेबसी को जैसे ठिकाने लगा देती है। प्रायः नगण्य सामारिक उपलब्धियों या अपनी राजनीतिक स्थितियों की दृष्टि से अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इतिहासकार भले ही एक कमज़ोर शासक के रूप में चित्रित करते हों लेकिन -गाजियों में बू रहेगी ज
No posts
No posts
No posts
No posts

Comments