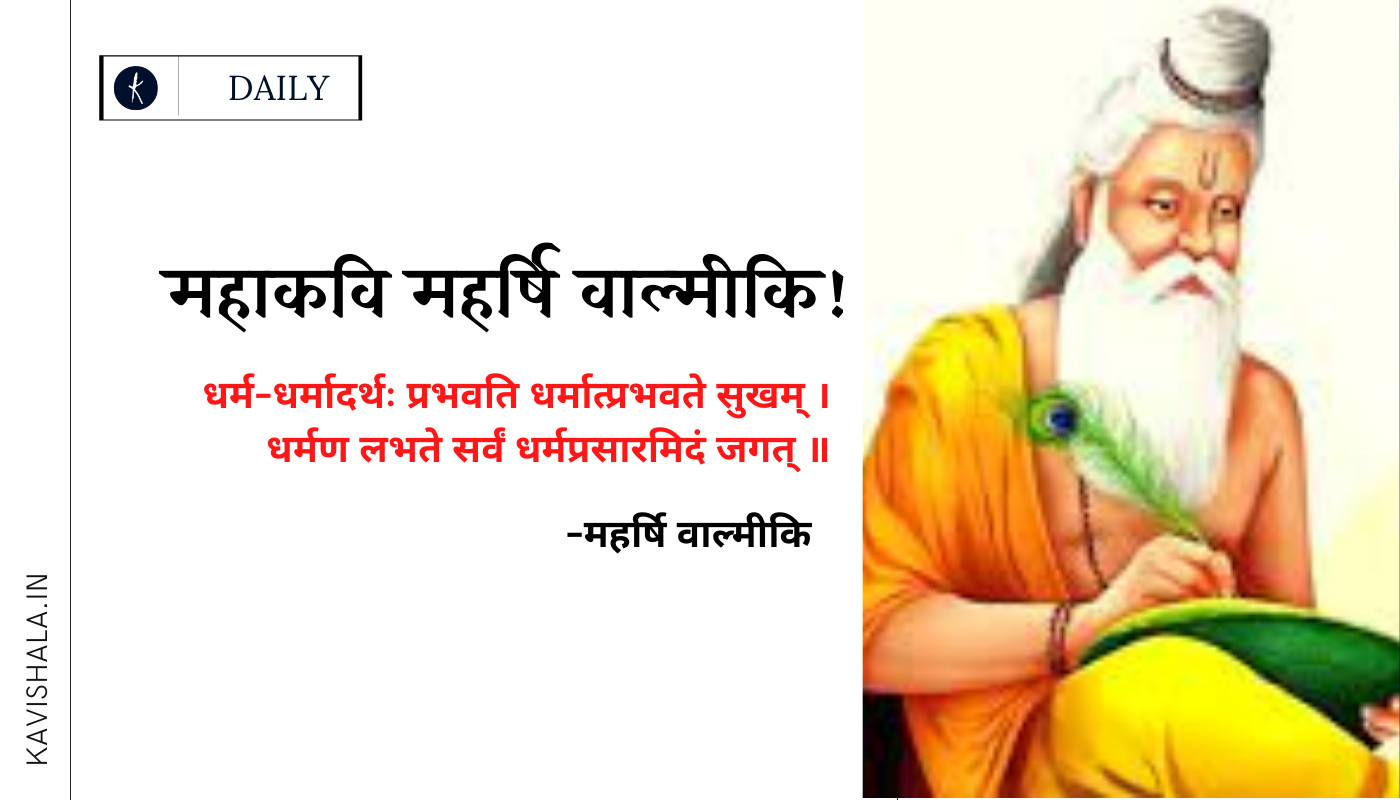
आदि कवि महर्षि वाल्मीकि - जब क्रोध में निकला प्रथम संस्कृत श्लोक ।
 October 20, 2021
October 20, 2021विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ “रामायण” की संस्कृत भाषा में रचना करने वाले श्रेष्ठम कवि महर्षि वाल्मीकि का जन्म हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार अश्विन पूर्णिमा को हुआ था और इसी दिन को महर्षि वाल्मीकि की जयंती के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर वाल्मीकि जयंती को प्रगति दिवस के नाम से भी जाना जाता है।
संस्कृत भाषा के प्रथम कवि:
महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि या संस्कृत भाषा के प्रथम कवि के रूप में स्थान प्राप्त है वहीं पहले संस्कृत श्लोक के रचनाकार भी महर्षि बाल्मीकि है थे । ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से भगवान राम की कहानी सुनी जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि को श्री राम के जीवन की हर घटना का ज्ञान हुआ। इसी आधार पर उन्होंने “रामायण” ग्रंथ की रचना की। बात करें इस महान ग्रन्थ की इसमें कुल 24000 श्लोक है और 7 अध्याय है जो कांड के नाम से जाने जाते है। इस ग्रंथ से त्रेता युग की सभ्यता, रहन सहन, सस्कृति की पूरी जानकारी मिलती है।
नारद मुनि बने मार्गदर्शक :
महर्षि वाल्मीकि महर्षि कश्यप और अदिति के नौवें पुत्र “वरुण” के पुत्र थे जो आगे चल कर एक एक महान तपस्वी थे परन्तु यह अचंभित करदेने वाला मत है की वे अपने जीवन के आरम्भिक काल में “रत्नाकर” नाम के डाकू थे जो लोगो को मारने के बाद उनको लूट लिया करते थे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।
कहा जाता है कि एक बार इन्होने नारद मुनि को बंदी बना लिया था जिस पर नारद ने पूछा कि ऐसा पाप कर्म क्यों करते हो? जवाब में रत्नाकर बोले “अपने परिवार के लिए?” नारद पूछने लगे कि क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पाप का भागीदार बनेगा। “हाँ, बिलकुल बनेगा” रत्नाकर बोले।
इस पर नारद मुनि ने उससे कहा की “अपने परिवार से पूछकर आओ क्या वो तुम्हारे पाप कर्म के भागीदार बनेगे। अगर वो हाँ बोलेंगे तो मैं तुमको अपना सारा धन दे दूंगा”। लेकिन जब रत्नाकर घर जाकर वही सवाल करने लगे तो किसी ने हाँ नहीं की उसके इस पाप में भागीदारी बनने के लिए। जिस्सके बाद बाल्मीकि का सम्पूर्ण जीवन बदल गया और पाप का रास्ता छोड़ कर तपस्या का रास्ता चयन किया। नारद मुनि ने इनका ह्रदय परिवर्तन किया था और श्री राम का भक्त बना दिया था। वर्षों तक गहन तपस्या करने के बाद एक दिवस आकाशवाणी हुई और उनका नाम बाल्मीकि हुआ। ब्रह्मदेव ने ज्ञान दिया और रामायण लिखने की प्रेरणा दी।
संस्कृत प्रथम श्लोक :
महर्षि बाल्मीकि ने संस्कृत व् अपना प्रथम श्लोक एक श्राप के रूप में दिया था जब एक दिन वाल्मीकि गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें तमसा नदी दिखी जिसका जल काफी स्वच्छ था। उन्होंने सोचा कि क्यों न यहां ही स्नान किया जाए। इसी दौरान उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा जो प्रणय-क्रिया में लीन था। उन्हें देखकर महर्षि वाल्मीकि को भी काफी प्रसन्नता हुई। लेकिन तभी अचनाक एक बाण आकर नर पक्षी को लग गया। वह तड़पते-तड़पते वृक्ष से गिर गया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। यह देख वाल्मीकि जी बेहद दुखी हुए और घटना से क्षुब्ध होकर उनके के मुंह से अचानक ही बहेलिए के लिए एक श्राप निकल गया जो इस प्रकार था :
मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।
यत्क्रौंचमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् ॥
और यही श्लोक रामायण का पहला
No posts
No posts
No posts
No posts
Comments