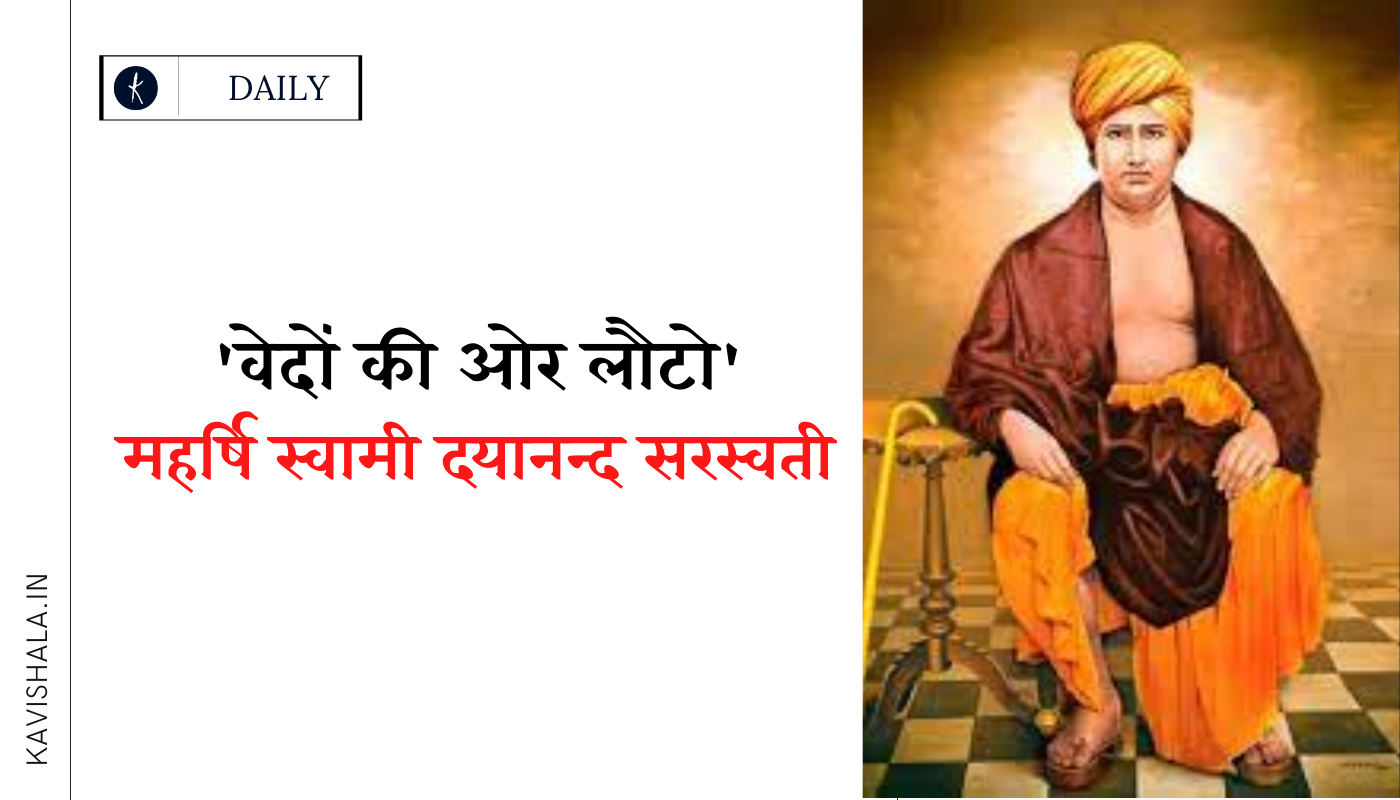
वेदों को छोड़ कर कोई अन्य धर्मग्रन्थ प्रमाण नहीं है
-दयानन्द सरस्वती
वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वंत्रता दिलाने के लिए मुम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की करने वाले सन्यासी दयानन्द सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिन्तक एवं समाज-सुधारक थे। दयानन्द सरस्वती वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि मानते थे उन्होंने वेदो का भाष्या किया जिस के कारण उनको ऋषि के नाम से सम्बोधित किया गया। दयानन्द सरस्वती ने कर्म सिद्धान्त, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा सन्यास को अपने दर्शन के चार स्तम्भ बनाया। उन्होने ही सबसे पहले १८७६ में 'स्वराज्य' का नारा दिया जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया।
उन्होंने कई नारों को जन्म दिया जिनमे वेदो की और लौटो प्रमुख है।
अपने विचारों से उन्होंने लाखों लोगो के जीवन को सदैव के लिए बदलने का कार्य किया वास्तव में तो उनके विचारों से प्रभावित महापुरुषों की संख्या अनगिनित है परन्तु मादाम भिकाजी कामा,भगत सिंह पण्डित लेखराम आर्य, स्वामी श्रद्धानन्द, चौधरी छोटूराम पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद 'बिस्मिल', महादेव गोविंद रानडे, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय इनमे कुछ प्रमुख नाम हैं।
बचपन में उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने दयानन्द को हिन्दू धर्म की परम्पराओं, मान्यताओं और ईश्वर के सन्दर्भ में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया।
उनके बचपन में एक घटना घाटी जिसके बाद उन्होंने ईश्वर पर ही संदेह हो गया। एक बार शिवरात्रि के महापर्व दिन उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मन्दिर में ही रुका हुआ था। सारे परिवार के सो जाने के पश्चात् भी वे जागते रहे यह सोच कर कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। परन्तु वास्तव में तो शिवजी के लिए रखे भोग को चूहे खा रहे हैं। यह देख कर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाये गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता वह हमारी क्या रक्षा करेगा! इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क दिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। इसके बाद उनके छोटी बहन की किसी कारण मृत्यु हो गए जिसका उन पर काफी प्रभाव पड़ा वे जीवन-मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता को उनकी चिंता होने लगी। बहुत रोकने पद भी वो नहीं रुके और 1846 में सत्य की खोज में निकल पड़े।सत्य की खोज के लिए उन्होंने अनेको स्थानों की यात्रा की , उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर 'पाखण्ड खण्डिनी पताका' फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशवचन्द्र सेन तथा देवेन्द्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिन्दी में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। यहीं उन्होंने तत्कालीन वाइसराय को कहा था, मैं चाहता हूं विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परंतु भिन्न-भिन्न भाषा, पृथक-पृथक शिक्षा, अलग-अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है
No posts
No posts
No posts
No posts

Comments